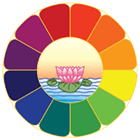अध्याय १
दो शक्तियां हैं जिनके मिलने से ही वह महत् और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है जो हमारे प्रयास का लक्ष्य है, एक है वह दृढ़ और अभंग अभीप्सा जो नीचे से आवाहन करती है और दूसरी वह भागवत प्रसादरूपा शक्ति जो ऊपर से उसका उत्तर देती है।
परंतु भागवत प्रसाद-शक्ति केवल प्रकाश और सत्य की ही स्थितियों में कार्य करती हैं; असत्य और अज्ञान उन पर जो अवस्थाएं लाद देना चाहते हैं उन अवस्थाओं में उनका कार्य नहीं होता। कारण असत्य जो कुछ चाहता है वह यदि उन्हें मंजूर हो जाये तो वे अपने ही व्रत से च्युत हो जायें।
प्रकाश और सत्य की स्थिति ही एकमात्र स्थिति है जिसमें वे परमा शक्ति नीचे उतर आती हैं; और विज्ञानमयी परमाशक्ति का ही यह काम है कि वे ऊपर से नीचे उतर कर और नीचे से ऊपर की ओर खुलकर इस भौतिक प्रकृति पर अपने अप्रतिहत कर्तृत्व का स्थापन और इसकी कठिनाइयों का ध्वंस कर सकती हैं। … होना चाहिये पूर्ण और सच्चा समर्पण, भागवती शक्ति की ओर अनन्य आत्मोद्घाटन, सत्य जो नीचे अवतरण कर रहा है उसका प्रतिपद, प्रतिक्षण अखण्ड ग्रहण और आये दिन पार्थिव प्रकृति का शासन किये चलनेवाले मनोगत, प्राणगत और देहगत आसुरी शक्तियों और रूपों के मिथ्यात्व का सतत सर्वथा परिवर्जन।
समर्पण होना चाहिये संपूर्ण, देही के एक-एक अंग और प्रत्यंग को लिये हुए। इतना ही यथेष्ट नहीं है कि हृत्पुरुष मान ले, आंतर मानस स्वीकार कर ले या अंतःप्राण नत हो जाये और देह की अंतश्चेतना भी उससे प्रभावान्वित हो; प्रत्युत पुरुष के किसी भी अंग में, बाह्यातिबाह्य अंग में भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये जिसमें किसी प्रकार का कोई संकोच हो, जो किसी प्रकार के संशय, व्यामोह और लुकाव-छिपाव के पीछे अपने-आपको छिपाये रहती हो, जो विद्रोही हो, समर्पण में असम्मत हो।
यदि सत्ता का कोई अंग समर्पण करे और कोई दूसरा अंग जहां-का-तहां अड़ा रह जाये, अपने ही रास्ते पर चलता चले या अपनी शर्तों को सामने रखे तो यह समझ लो कि जब-जब ऐसा होगा तब-तब तुम आप ही उस भागवती प्रसाद-शक्ति को अपने पास से दूर हटा दोगे।
यदि अपनी भक्ति और समर्पण के पीछे तुम अपनी इच्छाओं को, अहंकार की अभिलाषाओं और प्राणों के हठों को छिपा रखोगे, अपनी सच्ची अभीप्सा के स्थान में इन चीजों को ला रखोगे या अपनी अभीप्सा में इन्हें मिला दोगे तो यह समझ लो कि भगवत्प्रसाद-शक्ति का इसलिये आवाहन करना कि वे तुम्हारा रूपांतर करें, बिलकुल बेकार है।
यदि एक तरफ से या अपने एक अंग से तुम सत्य के सम्मुख होते हो और दूसरी तरफ से आसुरी शक्तियों के लिये अपने द्वार बराबर खोलते जाते हो तो यह आशा करना व्यर्थ है कि भगवत्प्रसाद-शक्ति तुम्हारा साथ देंगी। तुम्हें अपना मंदिर स्वच्छ रखना होगा यदि तुम चाहते हो कि भगवती जाग्रत् रूप से इसमें प्रतिष्ठित हों।
हर बार जब वे आती और सत्य को प्रविष्ट कराती हैं तब तुम यदि उनकी ओर पीठ फेर दो और फिर उसी मिथ्यात्व को बुला लो जिसका एक बार त्याग कर चुके हो तो ये भगवती का दोष नहीं जो वे तुम्हारा साथ न दें, बल्कि यह तुम्हारे अपने संकल्प के मिथ्याचार और तुम्हारे समर्पण की अपुर्णता का दोष है।
यदि तुम सत्य का आवाहन करते हो और फिर भी तुम्हारी कोई वृत्ति किसी ऐसी चीज को ग्रहण करती है जो मिथ्या, मूढ़ और अभागवत है अथवा ऐसी चीज का सर्वथा त्याग करना नहीं चाहती तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिये शत्रु को खुला रास्ता मिलता रहेगा और भगवत् प्रसादमयी भागवती शक्ति तुमसे पीछे हटती रहेंगी। पहले यह ढूंढ़ निकालो कि तुम्हारे अंदर कौन-सी चीज है जो मिथ्या या तमोग्रस्त है और उसका सतत त्याग करो; तभी तुम इस योग्य होगे कि ठीक तरह से भागवती शक्ति का इसलिये आवाहन करो कि वे आकर तुम्हारा रूपांतर साधित करें।
यह मत समझो कि सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अंधकार, समर्पण और स्वार्थ-साधन एक साथ उस गृह में रहने दिये जाएंगे जो गृह भगवान् को निवेदित किया गया हो।
रूपांतर होगा सर्वांगीण, इसलिये जो कुछ उस रूपांतर में बाधक है उसका त्याग भी होना होगा सर्वांगीण।
इस मिथ्या धारणा को त्याग दो कि तुम चाहे भगवन्निर्दिष्ट पथ पर न भी चलो तो भी भागवती शक्ति तुम्हारे लिये, तुम जब जैसा चाहोगे, सब कुछ किया करेंगी या उनको करना ही पड़ेगा। अपना समर्पण सच्चा और संपूर्ण करो, तभी तुम्हारे लिये बाकी सब कुछ किया जायेगा।
अज्ञान और आलस्य में पड़े-पड़े यह भी मत सोचो कि भागवती शक्ति ही तुम्हारे लिये समर्पण भी कर देंगी। भगवान् भागवती शक्ति के प्रति तुम्हारा आत्मसमर्पण चाहते हैं, पर जबर्दस्ती किसी से आत्मसमर्पण नहीं कराते; तुम्हारी स्वाधीनता सदा अक्षुण्ण है, जबतक रूपांतर-साधन उस अवस्था तक नहीं पहुंचता जहां से उसका च्युत होना असंभव है तबतक यह सर्वथा तुम्हारे अधिकार में है कि तुम जब चाहो भागवती शक्ति को अमान्य कर सकते हो या जब चाहो अपना समर्पण लौटा ले सकते हो, यदि उसका आध्यात्मिक फल भी भोगने को साथ-साथ तैयार हो। तुम्हारा समर्पण स्वेच्छाकृत और स्वच्छन्द होना चाहिये, किसी सजीव सत्ता का-सा, जड़ कठपुतली या परवश यंत्र का-सा नहीं।
प्रायः यह भूल हुआ करती है कि तामसिक निश्चेष्टता को वास्तविक समर्पण समझ लिया जाता है, पर तामसिक निश्चेष्टता से किसी भी सच्चे और शक्तिशाली पदार्थ का उद्भव नहीं हो सकता। अपनी तामसिक निश्चेष्टता के कारण ही भौतिक प्रकृति प्रत्येक तामस और आसुर प्रभाव का शिकार बना करती है।
भागवती शक्ति के कर्म करने के लिये साधक में उसके प्रति ऐसी अधीनता होनी चाहिये जो प्रसन्न, बलशाली और सहायक हो और ऐसी आज्ञाकारिता होनी चाहिये जो सत्य के ज्ञानदीप्त अनुयायी को, अंतर्जगत् में अंधकार और असत्य से लड़नेवाले वीर योद्धा को, भगवान् के सच्चे सेवक को शोभा दे।
यही सच्चा मनोभाव है और जो कोई इसे ग्रहण और धारण कर सकते हैं उन्हींकी श्रद्धा निराशाओं और विपत्तियों के बीच में भी सदा अटल बनी रह सकती है और वे ही इसकी कठिन अग्निपरीक्षा से उत्तीर्ण होकर उस परम विजय और चरम रूपांतर को प्राप्त हो सकते हैं।
अध्याय २
जगत् में जो कुछ भी होता है उसमें भगवान् अपनी शक्ति का आश्रय किये हुए, प्रत्येक कार्य के पीछे रहते हैं; पर यह उनका योगमाया से समावृत रहना है और इस अपरा प्रकृति में उनका जो कर्म होता है वह जीव के अहंकार के द्वारा होता है।
योग में भी भगवान् ही साधक हैं और साधना भी; ये उन्हींकी शक्ति हैं जो अपनी ज्योति, सामर्थ्य, ज्ञान, चैतन्य और आनंद से आधार (मन, प्राण, शरीर) के ऊपर अपना कर्म किये चलती हैं और जब यह आधार उनकी ओर उद्घाटित होता है तब वे ही अपनी इन दिव्य शक्तियों को उसमें भर देती हैं जिनसे साधना हो पाती है। परंतु जबतक निम्न प्रकृति सक्रिय है तबतक साधक के वैयक्तिक प्रयत्न की आवश्यकता रहती ही है।
यह वैयक्तिक प्रयत्न अभीप्सा, त्याग और समर्पण से युक्त त्रिविध अभ्यास है —
अभीप्सा — ऐसी जो अनिमिष, अविराम, अविच्छिन्न हो — मन में उसी का संकल्प, हृदय में उसी की खोज, प्राणों का वही अभिमत, देह की चेतना और प्रकृति को उसी की ओर उद्घाटित और सहज नम्य करने की दृढ़ इच्छा।
त्याग — अपरा प्रकृति की सब वृत्तियों का त्याग — मन की मान्यता, मत, अभिमत, अभ्यास, परिकल्पना, इन सबका ऐसा परित्याग कि जिससे रिक्त मन में वास्तविक ज्ञान को निर्बन्ध स्थान मिले — प्राण-प्रकृति की सारी वासना, कामना, लालसा, वेदना, आवेग, स्वार्थपरता, अहंकारिता, अहंमन्यता, लोलुपता, लुब्धता, ईर्ष्या, असूया, सत्य के प्रति विरुद्धाचार, इन सबका ऐसा त्याग कि स्थिर, उदार, समर्थ और समर्पित प्राण-सत्ता में वास्तविक शक्ति और आनंद की ऊपर से वर्षा हो — देह-प्रकृति की मूढ़ता, संशयग्रस्तता, अविश्वस्तता, अंधता, अनम्यता, क्षुद्रता, अलसता, परिवर्तन-विमुखता, तामसिकता, इन सबका ऐसा परिवर्जन कि ज्योति, शक्ति, आनंद की सत्स्थिरता निरन्तर अधिकाधिक दिव्य होनेवाली देह में सुप्रतिष्ठित हो ।
समर्पण — भगवान् और भगवती शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण — हम जो कुछ हैं और जो कुछ हमारे पास है, जो-जो हमारी चेतना है, जो-जो हमारी चित्तवृत्ति और गतिविधि है, इन सबका समर्पण।
*
समर्पण और आत्मनिवेदन में साधक जितना ही अग्रसर होगा उतना ही उसे इस बात का अनुभव होगा कि भागवती शक्ति ही साधना कर रही हैं, अपने-आपको उसके अंदर अधिकाधिक डाल रही हैं और उसमें दिव्य परा प्रकृति की स्वच्छन्दता और पूर्णता स्थापित कर रही हैं। जितना ही अधिक यह सचेत साधनक्रम उसके अपने प्रयास का स्थान अधिकृत कर लेता है उतनी ही द्रुत और वास्तविक उसकी साधनोन्नति होती है। परंतु इससे वैयक्तिक प्रयत्न की आवश्यकता का तबतक अंत नहीं होता जबतक समर्पण और आत्मनिवेदन सर्वांगतया नख से शिख तक विशुद्ध और संपूर्ण नहीं हो लेते।
यह बात ध्यान में रहे कि तामसिक भाव से किया हुआ समर्पण, जो समर्पण के विधानों का पालन करने से विमुख होता और सब कुछ करने के लिये भगवान् को ही पुकारता है, स्वयं कोई कष्ट उठाना और प्रयास करना नहीं चाहता — ऐसा समर्पण — केवल आत्मप्रवंचन है, इससे मुक्ति और सिद्धि नहीं प्राप्त होती।
अध्याय ३
जीवनपथ पर सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर आगे बढ़े चलने के लिये दो ही चीजें जरूरी हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं — एक है मां भगवती की करुणा और दूसरी, तुम्हारी ओर से ऐसा अंतःकरण जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से घटित हो। श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिये विशुद्ध, निश्छल और निर्दोष। मन और प्राण की ऐसी अहंकारयुक्त श्रद्धा जो बड़े बनने की आकांक्षा, अभिमान, दम्भ, अहंमन्यता, प्राण की स्वैरता, वैयक्तिक अभिलाष और निम्न प्रकृति की क्षुद्र वासनातृप्ति से कलंकित हो, ऊर्ध्वगमनाक्षम धूमाच्छन्न अग्निशिखा के समान है जो ऊपर स्वर्ग की ओर उज्ज्वलित नहीं हो सकती। अपने जीवन को यह समझो कि यह भगवत्कर्म के लिये और भगवान् के प्राकट्य में सहायक होने के लिये मिला हुआ है। और किसी चीज की इच्छा मत करो, चाहो केवल भागवत चैतन्यगत विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता, आनंद और उसका यह तकाजा कि उसके द्वारा तुम्हारा मन, प्राण, शरीर रूपांतरित हो, और कोई चीज मत चाहो, चाहो केवल भागवत, आध्यात्मिक और विज्ञानगत परम सत्य, उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर और तुम्हारे अंदर और उन सबके अंदर जो पुकारे गये और अनुगृहीत हुए हैं, और उस सत्य की सृष्टि के लिये आवश्यक अनुकूल परिस्थिति तथा समस्त विरोधिनी शक्तियों पर उसकी विजय।
तुम्हारी निष्ठा सच्ची और सर्वांगीण हो। जब आत्मनिवेदन कर रहे हो तो पूर्णतया ही करो; अपनी कोई इच्छा, कोई शर्त, कोई अलगाव मत रखो, जिसमें जो कुछ तुम्हारे अंदर है सब भगवती माता का हो और अहंकार के लिये कुछ भी शेष न रह जाये, न किसी अन्य शक्ति को कुछ दिया जाये।
तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने ही पूर्णतर होंगे उतनी ही अधिक दया तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम्हारी रक्षा होगी। और जब भगवती माता का वरद और रक्षक हाथ तुम्हारे ऊपर होगा तब फिर कौन है जो तुम्हारे ऊपर ऊंगली उठा सके या जिससे तुम्हें भय करना पड़े? इसकी अत्यल्प मात्रा भी तुम्हें सब विघ्न-बाधाओं और संकटों से पार कर देगी; इसकी पूर्ण सत्ता से घिरकर तुम अपने रास्ते पर निरापद आगे बढ़े चले जा सकते हो, क्योंकि यह रास्ता माता का है, यहां किसी विभीषिका की चिंता नहीं, किसी शत्रु का भय नहीं — वह चाहे कितना ही बलवान् हो, इस जगत् का हो या अन्य किसी अदृश्य जगत् का। माता के वराभयहस्त का स्पर्श कठिनाइयों को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणत कर देता है। कारण मां भगवती की दया भगवान् की अनुमति है और आज या कल उसका फल निश्चित है — पूर्वनिर्दिष्ट है, अवश्यंभावी और अकुंठ है।
अध्याय ४
धन एक विश्वजनीन शक्ति का स्थूल चिह्न है। यह शक्ति भूलोक में प्रकट होकर प्राण और जड़ के क्षेत्रों में कार्य करती है। बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिये इसका होना अनिवार्य है। इसके मूल और इसके वास्तविक कर्म को देखते हुए यह शक्ति भगवान् की है। परंतु भगवान् की अन्यान्य शक्तियों के समान यह शक्ति भी यहां दूसरों को सौंप दी गयी है और इस कारण अधःप्रकृति के अज्ञानान्धकार में इसका अहंकार के काम में अपहरण हो सकता है अथवा असुरों के प्रभाव में आकर विकृत होकर यह उनके काम आ सकती है। मानव अहंकार और असुर जिन तीन शक्तियों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और जो प्रायः अनधिकारियों के हाथों में पड़ जाती हैं तथा ये अनधिकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं उन्हीं आधिपत्य, धन और काम, इन तीन शक्तियों में से एक शक्ति है धन। धन के चाहनेवाले या रखनेवाले धन के स्वामी तो क्या होते हैं, अधिकतर धन के दास ही होते हैं। धन जो बहुत काल से असुरों के हाथों में रहा और इसका जो बराबर दुरुपयोग हुआ, इससे इस पर दोष की एक ऐसी गहरी छाप लगी हुई है कि उससे मुश्किल से कोई बचता हो। इसीलिये प्रायः सभी आध्यात्मिक साधन-मार्गों में पूर्ण संयम, अनासक्ति और धन के सब बंधनों तथा प्रत्येक प्रकार की वैयक्तिक और अहंकारयुक्त वित्तेषणा के त्याग पर इतना जोर दिया जाता है। कुछ साधन-मार्ग तो धन-वैभव को पाप ही समझते हैं और यह बतलाते हैं कि दरिद्रता और अपरिग्रह का होना ही आध्यात्मिक स्थिति है। पर यह भूल है, इससे यह शक्ति दानवी शक्तियों के हाथों में ही रह जाती है। इसका भगवान् के लिये पुनरुद्धार करना, क्योंकि यह भगवान् का है, और भागवत जीवन के लिये भागवत भाव से इसका उपयोग करना साधक का विज्ञानमूलक मार्ग है।
धनशक्ति और उससे प्राप्त होनेवाले साधनों और पदार्थों से तुम्हें वैरागियों की तरह न तो भागना चाहिये, न इनकी कोई राजसी आसक्ति या इनके भोग में पड़े रहने की दासत्व-वृत्ति ही पोसनी चाहिये। धन को केवल यह समझो कि यह एक शक्ति है जिसे माता की सेवा के लिये जीतकर लौटा लाना और उन्हींकी सेवा में अर्पण करना है।
सारा धन भगवान् का है और यह जिन लोगों के हाथ में है वे उसके ट्रस्टी (रक्षक) हैं, मालिक नहीं। आज यह उनके पास है, कल कहीं और चला जा सकता है। जबतक यह इनके पास है तबतक ये इस ट्रस्ट का पालन कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस बुद्धि से उसका उपयोग करते हैं और किस काम में करते हैं — इसी पर सब कुछ निर्भर करता है।
अपने लिये जब तुम धन का उपयोग करो तब जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो उसे माता का समझो। स्वयं कुछ भी मत चाहो पर वे जो कुछ दें उसे स्वीकार करो और उसी काम में उसे लगाओ जिसके लिये वह तुम्हें दिया गया हो। नितांत निःस्वार्थ, सर्वथा न्यायनिष्ठ, ठीक-ठीक हिसाब रखनेवाले, तफसील की एक-एक बात का ध्यान रखनेवाले उत्तम ट्रस्टी बनो; सदा यह ध्यान रखो कि तुम जिस धन का उपयोग कर रहे हो वह उनका है, तुम्हारा नहीं। फिर, उनके लिये जो कुछ तुम्हें मिले उसे श्रद्धा के साथ उनके सामने रखो; अपने या और किसी के काम में उसे मत लगाओ।
कोई मनुष्य धनी है केवल इसीलिये उसके सामने सिर नीचा मत करो; उसके आडम्बर, शक्ति या प्रभाव के वशीभूत मत हो। माता के लिये जब तुम किसी से कुछ मांगो तो तुम्हें यह प्रतीत होना चाहिये कि माता ही तुम्हारे द्वारा अपनी वस्तु का किंचित् अंश मात्र मांग रही हैं और जिस व्यक्ति से इस तरह मांगा जायेगा वह इसका क्या जवाब देता है उसी से उसकी परीक्षा होगी।
यदि धन के दोष से तुम मुक्त हो पर साथ ही संन्यासी की तरह उससे भागते नहीं हो तो भागवत कर्म के लिये धन जय करने की बड़ी क्षमता तुम्हें प्राप्त होगी। मन का समत्व, किसी स्पृहा का न होना और जो कुछ तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम्हें मिलता है और तुम्हारी जितनी भी उपार्जन-शक्ति है उसका भागवती शक्ति के चरणों में तथा उन्हींके कार्य में सर्वथा समर्पण, ये ही लक्षण हैं धनदोष से मुक्त होने के। धन के संबंध में या उसके व्यवहार में किसी प्रकार की मन की चंचलता, कोई स्पृहा, कोई कुण्ठा किसी-न-किसी दोष या बंधन का ही निश्चित लक्षण है।
इस विषय में उत्तम साधक वही है जो दरिद्रता में रहना आवश्यक होने पर वैसा रह सके और उसे किसी अभाव की कोई वेदना न हो या उसके अंदर भागवत चैतन्य के अबाध क्रीडन में कोई बाधा न पड़े; और वैसे ही यदि उसे भोग-विलास की सामग्री के बीच में रहना पड़े तो वह वैसा भी रह सके और कभी एक क्षण के लिये भी अपने धन-वैभव या भोग-विलास के साधनों की इच्छा या आसक्ति में न जा गिरे, असंयम का दास न हो अथवा धन रहने पर जैसी आदतें पड़ जाती हैं उनसे बेबस न हो जाये। भागवती इच्छा और भागवत आनंद ही उसका सर्वस्व है।
विज्ञानकृत सृष्टि में धनबल भागवती शक्ति को पुनः प्राप्त करा देना होगा और मां भगवती अपनी सृष्टि-दृष्टि की प्रेरणा से जो प्रकार निर्धारित करेंगी उसी प्रकार से उसका विनियोग एक नवीन दिव्यीकृत प्राणिक और भौतिक जीवन के सत्य सुंदर सुसंगत संघटन और सुव्यवस्थापन में करना होगा। पर पहले यह धनशक्ति उनके लिये जीतकर लौटा लानी होगी और इस विजय-संपादन में वे ही सबसे अधिक बलवान् होंगे जो अपनी प्रकृति के इस हिस्से में सुदृढ़, उदार और अहंकार-निर्मुक्त हैं, जो कोई प्रत्याशा नहीं करते, अपने लिये कुछ बचाकर नहीं रखते या किसी संकोच में नहीं पड़ते, जो परमा शक्ति के विशुद्ध वीर्यवान् यंत्र हैं।
अध्याय ५
यदि तुम भागवत कर्म के सच्चे कर्मी बनना चाहते हो तो तुम्हारा पहला लक्ष्य यही होना चाहिये कि तुम वासना मात्र से, तथा अपने-आपको ही सर्वस्व माननेवाले अहंकार से सर्वथा विनिर्मुक्त हो जाओ। तुम्हारा समस्त जीवन भगवान् के प्रति पुष्पाञ्जलि और यज्ञाहुति हो; कर्म में तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य हो भागवती शक्ति की लीला में उनकी सेवा करना, उन्हें धारण करना, कृतार्थ करना और उनके प्राकट्य का यंत्र बनना। तुम्हें भागवत चैतन्य से चैतन्य होना होगा, यहांतक कि तुम्हारी इच्छा और भगवती की इच्छा में कोई भेद न रह जाये, तुम्हारे अंदर उनकी प्रेरणा के अतिरिक्त और कोई संकल्प ही न उठे, कोई कर्म ऐसा न हो जो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा होनेवाला उन्हींका चिन्मय कर्म न हो।
जबतक तुम इस संपूर्ण सक्रिय अभेद के अधिकारी न हो सको तबतक तुम्हें अपने-आपको माता की सेवा के लिये सृष्ट वह जीव और देह समझना चाहिये जो माता के लिये ही सब कर्म करता है। पृथक् कर्तृत्वबोध यदि तुम्हारे अंदर प्रबल भी हो और तुम यह अनुभव करो कि कर्म करनेवाला कर्ता तो मैं ही हूं तो भी कर्म करो माता के लिये ही। अहंकार की पसंद का सारा जोर, वैयक्तिक लाभ की सारी लोलुपता, स्वार्थैकदृष्टिवाली कामना का सारा निबन्धन इन सबको मिटा देना होगा प्रकृति में से। कोई फलेच्छा न रह जाये, पुरस्कार पाने की कोई कामना प्रवेश न करे; एकमात्र फल तुम्हारे लिये हो मां भगवती की प्रसन्नता और उनके कर्म की सांग सम्पन्नता, एकमात्र पुरस्कार तुम्हारे लिये हो भागवत चैतन्य और शांति और सामर्थ्य और आनंद की तुम्हारे अंदर निरंतर वृद्धि। सेवा का आनंद और कर्म के द्वारा आंतरिक विकास का आनंद ही निरहंकार कर्मी के लिये यथेष्ट प्रतिफल है।
पर एक समय आयेगा जब तुम अधिकाधिक यह अनुभव करोगे कि तुम केवल यंत्र हो, कर्मी नहीं। कारण पहले तो तुम्हारे भक्तिबल से भगवती माता के साथ तुम्हारा संबंध इतना घनिष्ठ हो जायेगा कि जब चाहे उनका ध्यान एकाग्र करते ही और सब कुछ उनके हाथों में सौंपते ही तुम्हें उनका सद्यःनिर्देश, प्रत्यक्ष आदेश या प्रेरक भावविशेष प्राप्त होगा, इस बात का अति स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिये, किस तरह करना चाहिये और उसका क्या फल होगा। और फिर इसके बाद तुम यह अनुभव करोगे कि भगवत्-शक्ति केवल प्रेरणा और आदेश-निर्देश ही नहीं करती बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रवर्त्तन और उद्यापन भी वे ही करती हैं; तुम्हारी सारी वृत्तियां और गतियां उन्हींसे निकलती हैं, तुम्हारी सारी शक्तियां उन्हींकी हैं, तुम्हारे मन, प्राण, शरीर उन्हींके कर्म के सचेत सानन्द यंत्र हैं, उनकी लीला के उपकरण हैं, स्थूल जगत् में उनके प्राकट्य के पात्र हैं। ऐसी एकता और निर्भरता की अपेक्षा अधिक सुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती; इसमें प्रवेश होने पर तुम अज्ञान के संघर्ष-संकुल दुःखमय जीवन की सीमा पार कर फिर से अपनी आत्मसत्ता के सत्य में, उसकी गंभीर शांति और प्रगाढ़ आनंद में आ जाओगे।
जब कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार रूपांतर-साधन हो रहा है तब यह बहुत ही आवश्यक है कि तुम अपने-आपको अहंकार के समस्त विकृति-दोषों से विनिर्मुक्त रखो। कोई मांग, कोई हठ लुका-छिपा तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारे आत्मदान और आत्मोत्सर्ग की निर्मलता को कलंकित न करे। कर्म में या कर्मफल में कोई आसक्ति न हो, अपनी कोई शर्त न हो, जिस भगवत्-शक्ति से अधिकृत होकर रहना इष्ट है उस पर अपने अधिकार का दावा न हो, तुम भगवती के यंत्र हो इस बात का भी कोई घमण्ड न हो, किसी प्रकार की दाम्भिकता या उद्धतता न हो। मन, प्राण या देह के किसी अंग-प्रत्यंग में कोई ऐसी बात न रहे जो तुम्हारे अंदर कर्म करनेवाली महती शक्तियों की उस महत्ता को अपने काम में प्रयुक्त कर विकृत कर दे या अपनी ही व्यष्टिगत पृथक् संतुष्टि के साधन में लगा दे। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और विमल अभीप्सा अनन्यगतिक और तुम्हारी सत्ता के सब स्तरों और क्षेत्रों में व्यापक हो; जब ऐसा होगा तब सब प्रकार के क्षोभ और विकार उत्पन्न करनेवाली सब वृत्तियां-प्रवृत्तियां प्रकृति से क्रमशः झड़ जायेंगी।
इस सिद्धि की चरम अवस्था तब होगी जब तुम भगवती माता के साथ पूर्णतया एकीभूत हो जाओगे और अपने आपको कोई पृथक् सत्ता, यंत्र, सेवक या कर्मी न जानोगे बल्कि यह अनुभव करोगे कि तुम सचुमच ही माता के शिशु हो, उन्हींकी चेतना और शक्ति के सनातन अंश हो। सदा ही वे तुम्हारे अंदर रहेंगी और तुम उनके अंदर; तुम्हारी यह सतत, सहज, स्वाभाविक अनुभूति होगी कि तुम्हारा सब सोचना-समझना, देखना-सुनना और कर्म करना, तुम्हारा श्वास-प्रश्वास और तुम्हारे अंग-प्रत्यंग का हिलना-डोलना भी उन्हींसे होता है, वे ही करती हैं। तुम यह जानोगे, देखोगे और अनुभव करोगे कि उन्होंने ही तुम्हें एक व्यक्ति और शक्ति के रूप में अपने अंश से निर्मित किया है, अपने अंदर से लीला के हेतु बाहर प्रकट किया है और फिर भी सदा ही तुम उन्हींके अंदर सुरक्षित हो, उन्हींकी सत्ता से सत् हो, उन्हींके चैतन्य से चित् हो, उन्हींके आनंद से आनंद हो। यह स्थिति जब पूर्ण होगी और उनकी विज्ञान-तेजोराशि तुम्हारा अबाध परिचालन कर सकेगी तब तुम भागवत कर्म के सिद्ध कर्मी बनोगे; ज्ञान, संकल्प, कर्म तब सिद्ध, सहज, ज्योतिर्मय, स्वतःस्फूर्त, निर्दोष होंगे, भगवान् से ही उनका प्रवाह निःसृत होगा, सनातन का ही वह दिव्य शाश्वत कर्म होगा।
अध्याय ६
माता की चार शक्तियां उनके चार प्रधान व्यक्त रूप हैं, उनके दिव्य स्वरूप के अंश और विग्रह। इनके द्वारा वे अपने सृष्ट जीव-जगत् पर कर्म किये चलती, विभित्र लोकों में अपने सृष्टि-कर्मों को सुव्यवस्थित और सुसमन्वित करती और अपनी सहस्रों शक्तियों का गति-विधान करती हैं। माता हैं एक ही, पर हमारे सामने वे नाना रूप से आविर्भूत होती हैं; उनकी अनेकानेक शक्तियां और मूर्तियां हैं, अनेकों उनके स्फुलिंग और विभूतियां हैं जिनके द्वारा उन्हींका कर्म ब्रह्माण्ड में साधित हुआ करता है। वे जो एका हैं जिन्हें माता कहकर हम पूजते हैं, भागवती चिच्छक्ति हैं, अखिल विश्व की अधिष्ठात्री देवी। एका होती हुई भी वे इतनी अनेकरूपा हैं कि उनकी गति को देखना समझना अति क्षिप्र मन या सर्वथा विनिर्मुक्त परम व्यापक बुद्धि के लिये भी असंभव है। माता भगवती परम पुरुष भगवान् की चिति और शक्ति हैं और अपनी यावतीय सृष्टि के बहुत ऊपर स्थित हैं। परंतु उनकी गति का कुछ आभास मिलता और अनुभव होता है उनके विग्रहों से तथा जिन देविमूर्तियों में आकर वे अपने सृष्ट जीवों के सामने प्रकट होना स्वीकार करती हैं उनसे, क्योंकि इनके गुण और कर्म अधिक निर्दिष्ट और मर्यादित होने के कारण अधिक बोधगम्य होते हैं।
जो चिन्मयी शक्ति हमें और इस अखिल ब्रह्माण्ड को धारण करती हैं उनके साथ एकत्व से संस्पर्श का जब तुम्हें अनुभव होगा तब तुम स्वानुभव से यह जान सकोगे कि मातृसत्ता त्रिविध है। वे विश्वातीता, आद्या परा शक्ति हैं; इस रूप में वे सब लोकों के ऊपर हैं और वहां से वे परम पुरुष भगवान् के नित्य अव्यक्त रहस्य के साथ सृष्टि का संबंध जोड़े रहती हैं। फिर वे विश्वव्यापिनी, समष्टि-रूपिणी महाशक्ति हैं जो इन सब जीव-जगतों की सृष्टि करती और इन अनंत गतियों और शक्तियों को धारण करती, उनमें समाये रहती, उन्हें पुष्ट और परिचालित करती हैं। फिर हैं वे व्यष्टिरूपिणी; इस रूप में वे अपनी सत्ता के उन दो बृहत्तर स्वरूपों को मूर्तिमान करती हैं, उनकी गतिविधि हमें प्रतीत कराती और उन्हें हमारे निकट कर देती हैं; ये ही हैं मनुष्य और भागवती प्रकृति के बीच मध्यस्था शक्ति।
अद्वितीय आद्या पराशक्ति के रूप में माता अखिल लोकसमूह के ऊर्ध्व में स्थित हैं और परम पुरुष भगवान् को अपने सनातन चैतन्य में धारे हुई हैं। बस, उन्हीं में अशेष विशेषातीत शक्ति और अनिर्वचनीय सत्ता समायी हुई है; जिन सत्यों को व्यक्त करना होता है उनका समावेश या समाह्वान करके वे उन्हें परम रहस्य में उनकी अंतर्निहित अवस्था से अपने असीम चैतन्य के प्रकाश में उतार लाती हैं और उन्हें अपनी सर्वविजयिनी शक्ति और अपार प्राणधारा से एक-एक शक्ति और एक-एक शरीर इस विश्व में प्रदान करती हैं। पुरुषोत्तम इनके अंदर सदा ही अखण्डानन्त सच्चिदानन्दरूप से प्रकट हैं, इन्हींके द्वारा वे अखिल लोकसमूह में ईश्वर-शक्ति के द्वैताद्वैत चैतन्यरूप में और पुरुष-प्रकृति के द्वैत-तत्त्वरूप में प्रकट हुए हैं, इन्होंने ही उन्हें समस्त लोकों और भुवनों, देवताओं और उनकी शक्तियों के रूप में मूर्तिमान् किया और इन्हींके लिये वे ज्ञाताज्ञात लोकों में जहां जो कुछ है उस आकारवाले बने हैं। यह सारी लीला है इन्हींकी भगवान् पुरुषोत्तम के साथ; सनातन के जो रहस्य हैं, अनन्त के जो चमत्कार हैं, उन्हींका यह सारा प्रकटीकरण है। यह सब ये ही हैं; कारण सभी भागवती चिच्छक्ति के अंश और अच्छेद्य अंग हैं। यहां या कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो इनके द्वारा निर्दिष्ट और परम पुरुष भगवान् के द्वारा अनुमत न हो; केवल वही वस्तु रूपान्वित हो सकती है जिसे परम पुरुष की प्ररेणा से चालित होकर इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हो और अपनी सृष्टि के आनंद में बीजरूप में डालकर आकार प्रदान किया हो।
परम पुरुष से इनकी विश्वातीत पराचेतना के द्वारा जो-जो कुछ प्राप्त होता है, महाशक्ति विश्वजननी विश्वेश्वरी उसी की सृष्टि करती हैं और इस प्रकार जिन-जिन लोकों की सृष्टि करती हैं उनमें स्वयं भी अनुप्रविष्ट होती हैं; इनकी सत्ता इन लोकों में भागवत भाव और भागवत पोषणशक्ति और आनंद भर देती और उन्हींसे उन्हें बनाये रहती हैं — इन भागवत भाव, शक्ति और आनंद के बिना इन लोकों का अस्तित्व ही असंभव होता। जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं वह इन महाशक्ति का बाह्यतम कर्माङ्ग मात्र है; महाशक्ति स्वयं ही अपनी शक्तियों और कर्म-पद्धतियों का संचालन और उनका सामंजस्य विधान करती हैं, प्रकृति के द्वारा जो कर्म होते हैं वे उन्हींकी प्रेरणा से होते हैं और हम लोग जो कुछ देखते-सुनते, अनुभव करते हैं या जो कुछ जीवनधारा में लाया जा सकता है उसमें गुप्त अथवा प्रकट रूप से वे ही विचरती हैं। प्रत्येक लोक महाशक्ति की अखिल लोकसंस्थानलीला का एक-एक अभिनय है और महाशक्ति उन्हीं विश्वातीता परमा माता की ही विश्वभूता आत्मसत्ता और विश्वरूपा विश्वेश्वरी हैं। प्रत्येक लोक वह वस्तु है जिसे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि में देखा और अपने सौंदर्यमय और शक्तिमय हृदय में धारण किया और अपने आनंद में निर्मित किया है।
परंतु उनकी सृष्टि के अनेक स्तर हैं, भागवती शक्ति के अनेक पादपीठ हैं। हम लोग जिस लोक के अंग हैं उसके शिखर पर अनंत सत्ता, चेतना, शक्ति और आनंद के अनेक लोक हैं और उन सबके ऊपर माता खड़ी हैं अनावृत शाश्वत शक्तिरूप में। वहां सब सत्ताएं एक अनिर्वचनीय पूर्णता और अव्यभिचारिणी एकता में वास और विहार करती हैं, क्योंकि वहां माता ही उन्हें अपनी गोद में सदा निरापद लिये रहती हैं। इन लोकों की अपेक्षा अधिक समीप हमारे सर्वाङ्गपूर्ण विज्ञानसृष्टि के लोक हैं जहां माता विज्ञानमयी महाशक्ति, सर्वज्ञ संकल्प और सर्वशक्तिमान् ज्ञानस्वरूपिणी भागवती शक्ति विराजती हैं जो अपने सिद्ध कर्मों में नित्य प्रकट है और प्रत्येक प्रक्रिया में स्वभावतः ही सिद्ध हैं। वहां के सब व्यापार सत्य के पदक्षेप हैं; वहां के सब जीव भगवज्योति के ही जीवभूत अंश, शक्तिसमूह और शरीर हैं; वहां के सब अनुभव प्रगाढ़, अबाध आनंद के ही समुद्र, सप्लव और तंरग हैं। पर यहां जहां हम लोग रहते हैं, अज्ञानमय जगत् हैं, मन प्राण देह के लोक, जो अपनी चेतना में अपने उद्गमस्थान से विच्छिन्न हो गये हैं और यह पृथ्वी इनका एक विशेष अर्थपूर्ण केंद्र है जिसका विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक कठिनाइयां हैं — उन कठिनाइयों में से होकर तथा उन्हें दूर करते हुए लक्ष्य की ओर इसकी गति निर्धारित होती है। इसमें इतना अज्ञान और परस्पर-विरोध और प्रमाद भरा हुआ होने पर भी इसे धारण किये रहती हैं विश्वजननी; इसे भी इसके गुप्त लक्ष्य की ओर अग्रसर कराके ले जा रही हैं वे ही महाशक्ति।
अज्ञान के इस त्रिसर्ग की अधिष्ठात्री महाशक्तिरूपिणी माता अधिष्ठित हैं एक मध्यवर्ती लोक में जिसके ऊपर है वह विज्ञानमयी ज्योति, सत्यमय जीवन और सत्यात्मक सर्ग जिसे वहां से यहां नीचे ले आना है, और नीचे की ओर हैं चेतनाभेद से विभिन्न श्रेणियों में बंटे हुए ये चढ़ते और उतरते हुए चेतन क्षेत्र जो किसी दोहरी सीढ़ी के समान एक ओर से नीचे उतरकर जड़ के अज्ञान में परिसमाप्त हो गये हैं और दूसरी ओर से प्राण, हृदय और मन को प्रस्फुटित करके चढ़ गये हैं परमात्मा के अनन्तत्व में। माता वहां खड़ी हैं समस्त देवगणों के ऊपर, और वहां वे जो कुछ देखती, अनुभव करती और वर्षण करती हैं उसीसे इस ब्रह्माण्ड में और इस पार्थिव विकास में जो कुछ होगा उसका निर्देश कर देती हैं और उनके सब शक्तिसमूह और विग्रह अंदर से बाहर निकल आते हैं उनका कर्म करने के लिये और इनके तेज वे भेजती हैं इन अधोलोकों में शक्तिप्रयोग करने, शासन करने, युद्ध करने और विजयलाभ करने के लिये, यहां के युगचक्र निर्दिष्ट दिशा की ओर फेरने और घुमाने के लिये और समष्टिगत तथा व्यष्टिगत कर्मधाराओं को इष्ट मार्ग निर्दिष्ट करने के लिये। ये तेज ही वे अनेकानेक दिव्य रूप और विग्रह हैं जिनका अर्चन करके लोग इस रूप में विविध नामों से माता को सदा से पूजते आये हैं। परंतु इन शक्ति समूहों और इनके तेजों के द्वारा वे अपनी विभूतियों के मन और शरीर वैसे ही गढ़ा करती हैं जैसे वे ईश्वर की विभूतियों को गढ़ती हैं, इसलिए कि वे अपनी इन विभूतियों के द्वारा इस स्थूल भौतिक जगत् में मानवी चेतना के छद्मवेश में अपनी शक्ति, गुण और सत्ता की कोई आभा प्रकट कर दें। इस पार्थिव लीला के सब दृश्य किसी नाटक के समान उन्हीके द्वारा रचित, सज्जित और अभिनीत हैं, विश्वदेव इसमें उनके सहकारी हैं और वे स्वयं परदे के अंदर छिपी हुई अभिनेत्री हैं।
माता केवल ऊपर से ही विश्व का शासन नहीं करती बल्कि इस त्रिधाभिन्न निम्नतर जगत् में भी उतर आती हैं। उनकी निर्विशेष सत्ता के नाते, यहां की सब चीजें, अज्ञान की वृत्तियां तक भी स्वयं वे ही हैं और उन्हींके द्वारा सृष्ट हैं — यहां उनकी शक्ति अवश्य ही अवगुण्ठित है और सृष्ट पदार्थ अपने अपकृष्ट रूप में हैं, ये सब उन्हींकी प्रकृति-मूर्ति और प्रकृति-शक्ति हैं और इनके इस रूप में होने का कारण यह है कि अनंत की संभावनाओं में निहित किसी बात को कार्यान्वित करने के लिये, परम पुरुष की दुर्जेय अनुज्ञा से प्रवृत्त होकर वे यह महान् आत्मबलिदान करने को सम्मत हुई हैं और उसी लिये उन्होंने ये अज्ञान के अंतःकरण और रूप अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं। परन्तु विशेष सत्ता के नाते भी, वे करुणावश नीचे उतर आयी हैं इस अंधकार में इसलिये कि इसे प्रकाश की ओर ले जायें, इस मिथ्यात्व और प्रमाद में इसलिये कि इसे सत्य में परिवर्तित कर दें, इस मृत्यु में इसलिए कि इसे अमर जीवन में परिणत कर दें, इस संसारक्लेश और इसके दुरपनेय दुःख और यंत्रणा में इसलिये कि इसे अपने गभीर आनंद के रूपांतरकारी परमोल्लास में पर्यवसित कर दें। प्रगाढ़, प्रभूत अपत्यस्नेहवश ही उन्होंने तम का यह आवरण ओढ़ लेना स्वीकार किया है, अज्ञान और अनृत की शक्तियों के आक्रमण और उनके प्रभावों का अनेकविध उत्पीड़न सह लेना दयावश मंजूर किया है, जन्म जो मृत्यु का ही दूसरा नाम है उसके तोरण में से होकर निकलना सह लिया है, सृष्टि के सब क्लेश, शोक और दुःखभोग अपने ऊपर उठा लिये हैं, क्योंकि ऐसा देख पड़ा कि इसी एकमात्र उपाय से यह सृष्टि प्रकाश, आनंद, सत्य और सनातन जीवन की ओर उन्नीत की जा सकेगी। यही वह महान् आत्मबलिदान है जिसे विशेष-विशेष प्रसंग में पुरुषज्ञ कहा गया है पर जो गंभीरतर अर्थ में प्रकृति का आत्मस्वाहाकार है, भगवती माता का निःशेष आत्मयज्ञ।
माता इस विश्वब्रह्माण्ड का जो परिचालन और जगन्नाट्य-संबंधी जो कार्य करती हैं उसमें उनके चार महारूप विशेष रूप से सामने प्रकट हैं, ये उनकी प्रमुख शक्तियों और विग्रहों में से चार हैं। प्रथमा हैं उनकी विग्रहभूता प्रशांत विशालता, सर्वव्यापिनी ज्ञानवत्ता, अचंचल मङ्गलमयता, अशेष निःशेष करुणा, अतुल अद्वितीय महिमा और विश्वराट् गौरव-गरिमा। द्वितीया हैं मूर्तिमान् उनका भास्वर वीर्य और अदम्य आवेग, उनका रणोद्यत उन्मादभाव और सर्वजय संकल्प, उनका अति क्षिप्र प्रचण्ड वेग और प्रखर प्रलयंकर प्रताप। तृतीया हैं, कान्तिमयी, माधुर्यमयी और आश्चर्यमयी; सौंदर्य, सामंजस्य और छन्द-लालित्य का सारा निगूढ़ रहस्य उन्हीं में है; अति विचित्र और अति सूक्ष्म उनकी बहुविध संपदा है, दुर्निवार उनका आकर्षण और परम मनोहारिणी उनकी छवि है। चतुर्थी हैं उनकी आंतर ज्ञानवत्ता और सावधान निर्दोष कर्मकुशलता और समस्त विषयों में उनकी प्रशांत और यथावत् संसिद्धि की सहज अथाह क्षमता से विभूषिता मातृमूर्ति। ज्ञान, बल, सामंजस्य और संसिद्धि, माता के पृथक्-पृथक् विशिष्ट लक्षण हैं और इन्हीं शक्तियों को वे अपने साथ इस जगत् में ले आती हैं, अपनी विभूतियों में मानवीय आवरण को आश्रय कर उन्हें प्रकट करती हैं; और जो लोग माता के साक्षात् जीते-जागते प्रभाव की ओर अपनी पार्थिव प्रकृति को उद्घाटित कर रख सकेंगे उनमें वे अपनी ऊर्ध्व दिव्य स्थिति के धर्म के अनुसार अपनी इन शक्तियों को प्रतिष्ठित करेंगी। माता के इन महारूपचतुष्टय को हम इन चार महानामों से पुकारते हैं — महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।
राजराजेश्वरी महेश्वरी मानसी तर्कबुद्धि और इच्छाशक्ति के ऊपर बृहत् में आसीन हैं और वे इन दो वृत्तियों को विशुद्ध और उन्नत करके ज्ञानस्वरूप और बृहत् बनाती हैं अथवा परा ज्योति से प्लावित कर देती हैं। कारण वे ही हैं वे शक्तिमयी ज्ञानमयी जो हमें विज्ञान की अनंत सत्ताओं की ओर, विश्वव्यापक बृहत् की ओर, परमा ज्योति की माहेश्वरी महिमा की ओर, अलौकिक ज्ञान के भंडार की ओर और माता की चिरंतन शक्तियों की अपरिमेय गति की ओर उन्मुक्त कर देती हैं। शांतिमयी हैं, आश्चर्यमयी हैं, सदा अपनी महिमा में स्थित स्थिर-गंभीर। कोई चीज उन्हें हिला-डुला नहीं सकती, क्योंकि समग्र ज्ञान उनके अंदर है; कोई बात जो वे जानना चाहें उनसे छिपी नहीं रह सकती; सब पदार्थ और सब जीव और उनके स्वभाव और उनके चालक भाव तथा सृष्टि का विधान और उसके कालविभाग तथा यह जो कुछ जैसा था और है और होगा, सब उनके दृष्टिगत है। उनमें वह शक्ति है जो सबके सामने आती और सबको वश में करती है और कोई भी उनका विरोध करके उनके महान् अननुमेय ज्ञान और उत्तुंग प्रशांत शक्ति के सामने अंत तक ठहर नहीं सकता। वे सम हैं, धीर हैं, अपने संकल्प में अटल हैं, मनुष्यों के साथ उनका व्यवहार जिस-तिस की प्रकृति के अनुसार और पदार्थ मात्र तथा घटना मात्र में उनका कार्य उनकी शक्ति और अंतःस्थ सत्य के अनुरूप होता है। पक्षपात उनमें है ही नहीं, परंतु वे परम पुरुष भगवान् के आदेशों का अनुवर्तन करती हैं और इस तरह वे किसी को ऊपर उठाती हैं और किसी को ढकेल देती हैं नीचे या अपने पास से हटाकर अंधकार में डाल देती हैं। ज्ञानियों को वे और भी महान्, और भी ज्योतिर्मय ज्ञान प्रदान करती हैं; जिन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त है उन पर वे अपनी मंत्रणा का रहस्य प्रकट करती हैं, जो विरुद्धाचारी हैं उनसे उनके विरुद्धाचार का फल भोग कराती हैं; जो अज्ञ और मूढ़ है उन्हें उनकी अंधता के अनुसार ही लिये चलती हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के विभिन्न अंगों को वे तत्तत् अंग के प्रयोजन, प्रवृत्ति और वांछित प्रतिफल के अनुसार प्राप्त होती और उन्हें संचालित करती हैं; उनके ऊपर यथावश्यक भार रखती हैं अथवा उन्हें उनकी प्रिय पोषित स्वतंत्रता के हवाले कर देती हैं अज्ञान के मार्ग में फलने-फूलने या विनष्ट होने के लिये। कारण वे सबके ऊपर हैं, जगत् की किसी वस्तु में बद्ध या आसक्त नहीं। तथापि उन्हींका हृदय और सब की अपेक्षा, जगन्माता का हृदय है। उनकी करुणा अपार, अशेष है; सभी उनकी दृष्टि में उनके संतान और अद्वितीय एकमेव भगवान् के अंश हैं — असुर, राक्षस और पिशाच तक, और जो उनके विद्रोही और विरोधी हैं वे भी। वे यदि किसी का त्याग करती हैं तो उनका वह त्याग करना, कुछ काल पश्चात् अनुग्रह करने के निश्चय का ही एक प्रकार है और यदि वे किसी को दंड देती हैं तो उनका वह दंडविधान भी उनका प्रसाद ही है। परंतु उनकी करुणा उनके ज्ञान को अंध नहीं करती या उनके कर्म को निर्दिष्ट पथ से भ्रष्ट नहीं करती; कारण पदार्थ मात्र के सत्य से ही उनको काम है, ज्ञान ही उनकी शक्ति का केंद्र है और हमारे अंतरात्मा और प्रकृति को भागवत सत्य के अनुरूप निर्मित करना ही उनका व्रत और अनुष्ठान है।
महाकाली की प्रकृति और है। बृहत्ता नहीं बल्कि उत्तुंगता, ज्ञानवत्ता नहीं बल्कि शक्तिमत्ता और बलवत्ता उनकी अपनी विशेषता है, उनके अंदर एक अति तुमुल तीव्रता है, अति प्रचंड आवेग है कृतसंकल्प की पूर्ण सिद्धि का; एक दिव्य हिंसा-पिपासा है जो प्रत्येक सीमा और विघ्नबाधा को चूर्ण-विचूर्ण करने के लिये महावेग से प्रधावित होती है। उनका सारा दिव्यत्व उछल पड़ता है महारुद्र कर्म की रौद्री महाप्रभा के रूप में; वे हैं ही द्रुतता के लिये, सद्यःफलदायिनी कर्मपद्धति के लिये, क्षिप्र और ऋजु प्रहार के लिये, उस सम्मुखीन आक्रमण के लिये जो मैदान साफ करता जाता है। असुर के लिये उनका रूप बड़ा ही भयंकर है, भगवान् के द्रोहियों के लिये उनका चित्त बड़ा ही निर्मम और निदारुण है। कारण वे समस्त भुवनों की रणचंडी हैं जो रण से पश्चात्पद नहीं होतीं। कोई त्रुटि या दोष वे बर्दाश्त नहीं कर सकतीं, इसलिये मनुष्यों में जो कुछ ऐसा है जो अनुकूल नहीं होना चाहता उसके साथ उनका बड़ा कठोर व्यवहार होता है और जो कुछ ज्ञानहीन और तमोग्रस्त बना रहता है उसके साथ वे बड़ी निठुरता से पेश आती हैं; विश्वासघात, मिथ्याचार और ईर्षाद्वेष पर उनका कोप आशु और भीषण होता है, द्वेषबुद्धि पर तुरत उनके शूल का प्रहार होता है। भागवत कर्म में औदासीन्य, अवहेलन और आलस्य उन्हें सह्य नहीं और असमय सोनेवाले और समय पर काम न करनेवाले दीर्घसूत्री को, प्रयोजन होने पर, वे ताड़न से तीव्र वेदना उत्पन्न करके जगा देती हैं। जो भाव द्रुत, ऋजु और निष्कपट होते हैं, जो गतियां अकुंठ और अव्यभिचारिणी होती हैं, जो अभीप्सा उज्ज्वलित हो उठती है, वे सब महाकाली के संचार हैं। उनकी मनोवृत्ति अदम्य है, उनकी दृष्टि और इच्छाशक्ति श्येन पक्षी की उड़ान-सी ऊंची और बड़ी दूर तक फैली हुई होती है। ऊर्ध्व पथ में उनके पदक्षेप अति द्रुत होते हैं और उनकी भुजाएं मारने और तारने को आगे बढ़ी रहती हैं। कारण वे भी तो माता ही हैं और उनका स्नेह वैसा ही तीव्र है जैसा कि उनका क्रोध, और कारुण्य उनका अति गभीर और तुरत उमड़ पड़नेवाला होता है। जब उन्हें स्वसामर्थ्य के साथ कहीं भी दखल देने का अवसर मिलता है तब एक क्षण में संहतिविहीन पदार्थों के समान नष्ट हो जाती हैं वे सब बाधाएं जो साधक को आगे बढ़ने से लाचार किये रहती हैं और वे सब दस्यु भी मृतप्राय हो जाते हैं जो साधक पर आक्रमण किया करते हैं। उनका कोप विरोधियों को कंपानेवाला और उनके आवेश का भीषण भार दुर्बल और कातर को पीड़ा पहुंचानेवाला होता है, परंतु जो महान् बलवान् और सत्पुरुष हैं वे उनकी श्रद्धा भक्ति और पूजा करते हैं; क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि जो कुछ उनके विद्रोह का कारण है उसे ठोक-पीटकर वे समर्थ और निर्दोष सत्य बना देंगी, जो कुछ कुटिल और विपरीत है उसे वे अपने हथौड़े की चोट से सीधा कर देंगी और जो कुछ अशुद्ध और सदोष है उसे निकाल बाहर कर देंगी। उन्हींकी बदौलत यह बात है कि जो काम सदियों में होनेवाला होता है वह एक दिन में हो जाता है; इनके बिना आनंद महान् और गंभीर या मृदु मधुर और सुन्दर हो सकता है पर उस आनंद के जो परम कैवल्यस्वरूप तीव्रतम भाव हैं उनका प्रज्वलित उल्लास उसमें नहीं रह सकता। ज्ञान को वे ही विजयशालिनी शक्ति प्रदान करती हैं, सौंदर्य और सुसंगति को ऊर्ध्वमुखीन और ऊर्ध्वगामिनी गति प्रदान करती हैं और संसिद्धि के मंद और कष्टसाध्य साधन में वह वेग भर देती हैं कि जिससे साधक की शक्ति बहुगुणित होती और लंबा रास्ता छोटा हो जाता है। परतम आनंद, उच्चतम उच्चता, महत्तम लक्ष्य और विशालतम दृष्टि से न्यून किसी भी बात से उन्हें संतोष नहीं होता। इसलिये भगवान् की जो विजयिनी शक्ति है वह उन्हीमें है और उन्हींके तेज, आवेग और सत्वरता के प्रसाद से यह संभव है कि हमारे प्रयास की महत्सिद्धि किसी कालान्तर में नहीं, बल्कि अभी सत्वर साधित हो सकती है।
केवल ज्ञानवत्ता और शक्तिमत्ता ही परमा माता के प्रकटित वपु नहीं हैं; उनकी प्रकृति का और भी एक सूक्ष्मतर रहस्य है और उसके बिना ज्ञान और शक्ति अधूरे ही रह जाते हैं और पूर्णत्व भी उसके बिना पूर्ण नहीं होता। ज्ञान और शक्ति के ऊपर है शाश्वत सौंदर्य का परमाश्चर्य, भागवत समन्वय-निचय का एक ऐसा अगम्य रहस्य, अनिवार्य विश्वव्यापक रमणीयत्व और आकर्षण का एक ऐसा वशीकरण जो सब वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओं को एक जगह खींच लाता और पकड़ रखता है और उन्हें बलात् एक दूसरे से मिलाता और संयुक्त करता है जिसमें अंतर्हित आनंदविशेष अंतराल से ही अपना खेल खेले और उन्हें अपने छंद और रूप बनावे। यह महालक्ष्मी की शक्ति है और भागवती शक्ति का कोई रूप देहधारियों के हृदय के लिये इनसे अधिक आकर्षक नहीं है। महेश्वरी इतनी स्थिर-गंभीर, महीयसी और दूरवर्ती प्रतीत हो सकती हैं कि पार्थिव प्रकृति की क्षुद्रता उन तक पहुंचने और उन्हें धारण करने में समर्थ न हो सके, महाकाली भी इतनी द्रुतगामिनी और अट्टाल वासिनी भासित हो सकती हैं कि यह दुर्बल पार्थिव प्रकृति, उनका भीषण भार सह न सके; पर महालक्ष्मी की ओर सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दौड़ पड़ते हैं। कारण वे भगवान् की उन्मादन माधुर्य का जादू डालती हैं, उनके समीप होना गहरे आनंद में डूबना है और उन्हें अपने हृदय के अंदर अनुभव करना जीवन को आह्लादमय और कौतुकमय बना देना है; श्री, शोभा और रमणीय मृदुता उनसे वैसे ही प्रवाहित होती हैं जैसे सूर्य से प्रकाश, और जहाँ कहीं वे अपनी अनुपम दृष्टि गड़ाती हैं या अपना स्मितमाधुर्य टपकाती हैं वहीं मनुष्य वशीभूत होकर उनका दास बन जाता और अतल आनंद के तल में जा डूबता है। उनके करकमलों का स्पर्श अयस्कान्त का काम करता है और उनके अलौकिक कोमल प्रभाव से मन, प्राण, शरीर शुद्ध और परिमार्जित हो जाते हैं और जहां उनके पांव पड़ते हैं वहीं से बह निकलते हैं चित्तोन्मादन आनंद-सुरधुनि के स्रोत ।
तथापि इन मोहिनी शक्ति को प्रसन्न करना या उनकी सत्ता अपने अंदर बनाये रहना सहज नहीं है। अंतःकरण और अंतरात्मा का सामंजस्य और सौंदर्य, चिंता और अनुभूति का सामंजस्य और सौंदर्य, प्रत्येक बाह्य कर्म और गतिविधि में सामंजस्य और सौंदर्य, जीवन और जीवन के चतुःपार्श्व का सामंजस्य और सौंदर्य — यह है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अनुष्ठान। निगूढ़ जगदानन्द के छंदों के साथ जहां जीवन मिल जाता है, जहां सौंदर्यमय समग्र की पुकार पर चित्त दौड़ पड़ता है, जहां स्वरों का मेल है, ऐक्य है और अनेकानेक जीवनों का सानन्द प्रवाह भगवान् की ओर मुड़ा हुआ है वहां, वैसी ही स्थिति में, रहना वे मंजूर करती हैं। पर जो कुछ कुत्सित, गर्हित, घृणित है, जो कुछ निस्तेज, मलिन और अशुचि है, जो निर्दय और दुर्मुख है, वह उनके आगमन का प्रतिरोधी है। जहां प्रेम नहीं, सौंदर्य नहीं और इनके होने की गुंजायश भी नहीं, वहां वे नहीं आया करतीं; जहां प्रेम और सौंदर्य घृणित पदार्थों से मिलकर कुरूप बन जाते हैं वहां से वे तुरत अपना मुंह फेर लेती और बिदा होती हैं अथवा वहां वे अपना वैभव दान करने को उत्सुक नहीं होतीं। यदि वे अपने-आपको ऐसे मनुष्यों के हृदयों में अवस्थित देखती हैं जो स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष, असूया और कलह से घिरे हुए हैं, यदि विश्वासघातकता, लोभान्धता और कृतघ्नता मिली हुई है देवोद्दिष्ट अर्घ्यपात्र में, यदि तृष्णा की ग्राम्यता और अपवित्र काम भक्ति को अपमानित कर रहे हैं तो ऐसे हृदयों में दयामयी सौंदर्यमयी भगवती ठहर नहीं सकतीं। एक दैवी घृणा से उनका चित्त उचाट हो जाता और वे वहां से चल देती हैं, क्योंकि वे ऐसी नहीं हैं जो अपने ठहरने के लिये आग्रह करें या झगड़ती बैठी रहें; अथवा वे यह कर सकती हैं कि वहीं अंतर्धान होकर यह प्रतीक्षा करें कि इस पात्र में से यह कटु विषाक्त पैशाचिक दुर्भाव परित्यक्त होकर नष्ट हो जाये और तब इसमें अपना सुखद प्रभाव फिर से नवस्थापित किया जाये। संन्यासियों की-सी रिक्तता और रुक्षता उन्हें पसंद नहीं, न हृदय के गभीरतर उमंगों का दमन और न अंतरात्मा के और जीवन के सौंदर्यसाधक अंशों का कठोर उच्छेदन ही उन्हें सुहाता है। कारण प्रेम और सौंदर्य के द्वारा ही वे मनुष्यों को भगवत्पाश में बांधती हैं। उनके परम सृष्टिकर्म में जीवन स्वर्गीय कला का एक सर्वांगसुन्दर कारुशिल्प बनता और सारा जगत् एक दिव्य आनंद का काव्य बन जाता है; जगत् की सारी संपदा एक जगह लायी जाती और एक महत्तम व्यवस्थाक्रम में एकत्र प्रयुक्त होती है और उनकी अंतर्ज्ञानदृष्टि की साक्षात् एकत्वदर्शिता तथा उनके प्राणस्पर्श से अति सामान्य साधारण वस्तु भी अलौकिक बन जाती है। हृदय में उन्हें बैठाने से वे ज्ञान को समुन्नत आश्चर्य-शिखर पर पहुंचा देती हैं और समस्त ज्ञान के परे जो परमानन्द है उसके गुप्त रहस्य खोल-खोलकर दिखाती हैं, भक्ति को भगवान् की वेगवती आकर्षणशक्ति से लाकर मिला देती हैं, बलवत्ता और शक्तिमत्ता को वह छन्द सिखा देती हैं जिससे उनके कर्मों की सामर्थ्य सुसंगत और सुपरिमित बनी रहे और संसिद्धि पर वह मोहिनी डाल देती हैं कि जिससे वह चिरस्थायिनी हो जाती है।
महासरस्वती माता की कर्मशक्ति और सिद्धि और सुव्यवस्था में उनकी प्राणशक्ति हैं। शक्ति-चतुष्टय में ये सबसे कनिष्ठा और कर्म-संपादन में सबसे निपुण तथा स्थूल प्रकृति के लिये सबसे समीप हैं: महेश्वरी विश्वशक्तियों की बृहती धाराएं मात्र आंकती हैं, महाकाली उनकी गति और गति के वेग को आगे बढ़ाती हैं, महालक्ष्मी उनके छंद और मान उद्घाटित करती हैं, परंतु महासरस्वती उनके संपूर्ण संविधान और प्रयोग की एक-एक बात, एक-एक अंग के परस्पर-संबंध-प्रस्थापन और सब शक्तियों के सार्थक संयोजन तथा निश्चितार्थ की संप्राप्ति और संपूर्ण के विषय में अव्यर्थ यथायोग्य अनुष्ठान का पर्यवेक्षण करती हैं। सब विद्या, कला और कौशल महासरस्वती के साम्राज्यान्तर्गत हैं। सिद्ध कर्मी का अंतरंग और यथावत् ज्ञान, सूक्ष्म बोध और धैर्य, अंतर्ज्ञानी मन और सचेत हाथ और यथावत् गुणदोष दर्शी दृष्टि की प्रमादरहित सुनिश्चितता, सिद्धकर्मी के ये सब लक्षण महासरस्वती की प्रकृति में सदा ही अवस्थित रहते हैं और जिन पर वे अनुग्रह करती हैं उन्हें वे यह सारी संपदा प्रदान कर सकती हैं। ये शक्ति ही समस्त लोकों की समर्थ, अक्लान्त, सावधान, सुनिपुण निर्माणकर्त्री, व्यवस्थापिका, शासिका, प्रयोगज्ञानवती, कलावती और लोकविभागकर्त्री हैं। जब वे प्रकृति के रूपांतर और नवनिर्माण का कार्य अपने हाथ में लेती हैं तब उनका कार्य बड़ा ही श्रमसाध्य और बड़ी बारीकी के साथ होता है, हमारे अधीर चित्त को प्रायः बड़ा धीमा और जाने कब समाप्त होनेवाला-सा प्रतीत होता है, पर वह कार्य होता है अविराम, सर्वाङ्गीण और त्रुटिरहित। कारण कर्ममात्र में उनका संकल्प सुदक्ष, अतंद्रित और अश्रान्त होता है; वे हमारे ऊपर झुकी हुई हमें घेरे हुई रहती और जरा-जरा-सी एक-एक बात देखती और उसे स्पर्श करती हैं, बारीक से बारीक दोष, छिद्र, गांठ या न्यूनता को ढूंढ़ निकालती हैं और जो कुछ अबतक किया जा चुका है और जो कुछ आगे करना बाकी है उसे ठीक-ठीक समझती-बूझती और नापती-जोखती हैं। कोई भी चीज इतनी छोटी या तुच्छ नहीं है जो उनकी दृष्टि के सामने आने योग्य न हो, ऐसी भी कोई चीज नहीं है, चाहे वह कितनी ही झीनी, छद्मयुक्त या गुप्त हो, जो उनकी दृष्टि से बच सके। गढ़ना और फिर गढ़ना प्रत्येक अंग को, यही उनका सतत आयास है — जबतक वह अंग अपने सद्रूप को न प्राप्त हो, समग्र के अंदर अपने स्वस्थान में आकर न बैठ जाये और अपना नियत कर्म पूरा न करे। इस सतत अध्यवसाय के पूर्ण संघटन और पुनःसंघटन के कार्य में सब प्रयोजनों पर तथा जिस प्रयोजन की जिस प्रकार पूर्ति होगी उन सब प्रकारों पर एक साथ उनकी दृष्टि रहती है; वे अपनी अंतर्ज्ञानदृष्टि से यह जानती हैं कि कहां किस वस्तु को ग्रहण और किस वस्तु को वर्जन करना होगा और इस तरह सिद्धता के साथ वे योग्य पात्र, योग्य काल, योग्य अवस्था और योग्य प्रक्रिया का निर्देश करती हैं। अयत्न, अवहेलन और आलस्य से उन्हें घृणा है; कोई भी काम किसी तरह से निबटा देना, जल्दबाजी से कोई काम करना और उसका क्रम उलट पलट देना, सब तरह का भद्दापन, न्यूनाधिक्य लक्ष्यभ्रष्टता, करणों और गुणों का मिथ्यारोपण और दुरुपयोग, कार्य कर्मों को बिना किये या करके बीच में ही छोड़ देना, उनके स्वभाव के लिये अप्रियकर और सर्वथा विपरीत है। जब उनका कोई कार्य हो चुकता है तब यह देख पड़ता है कि उसमें कोई बात भूली नहीं है, कोई अंश अस्थान में नहीं जा पड़ा है, न कोई चीज छूटी है, न किसी में कोई दोष रह गया है; सारा काम पक्का, दुरुस्त, पूरा और देखने ही योग्य होता है। पूरी पूर्णता के बिना उन्हें चैन नहीं मिलता और अपने सृष्टिकर्म की परिपूर्णता के लिये अनन्त काल तक श्रम करना आवश्यक हो तो उसके लिये वे प्रस्तुत रहती हैं। इस कारण माता के शक्तिविग्रहों में सबसे अधिक ये ही मनुष्य और उसके सहस्रों दोषों को परम धैर्य के साथ सहती चली आयी हैं। सदया हैं, सुस्मिता हैं, हमारे अति समीप हैं और सदा सहाय हैं, सहसा विमुख या हताश होनेवाली नहीं, मनुष्य के बार-बार चूकने पर भी उसका बराबर साथ देती हैं, पद-पद पर उनका हाथ हमें सम्हाले रहता है यदि हमारा संकल्प अव्यभिचारी हो और हम निष्कपट और सच्चे हों; कारण द्विधा मन वे नहीं बर्दाश्त कर सकतीं और कलई खोल देनेवाला उनका विद्रूप झूठे स्वांग, छल-बलकौशल, आत्मप्रवंचना और पाखंड के लिये बड़ा ही निर्मम होता है। हमारे लिये जो-जो कुछ आवश्यक है उसे जुटा देनेवाली वे माता हैं, संकटकाल में सहायता करनेवाली सुहृद् हैं, धीर-गंभीर मंत्री और मन्त्रदात्री हैं, अपने भास्वर मन्दहास्य से विषाद, अवसाद और खिन्नता के बादल वे छिन्न-भिन्न कर देती हैं, नित्य-प्राप्त सहायता की सदा याद दिलाती हैं, अंगुली-निर्देश करती रहती हैं सदा उस स्थान की ओर जहां सूर्य-प्रकाश नित्य वर्तमान है और इस तरह दृढ़ता, अचंचलता और अध्यवसाय के साथ लगी रहती हैं उसी गभीर निरवच्छिन्न प्रेरणा में जो हमें परा प्रकृति की पूर्णता की ओर आगे बढ़ाये चलती है। अन्य सब शक्तियों के कार्य की संपूर्णता इन्हीं पर अवलंबित है; क्योंकि ये ही भौतिक आधार सुदृढ़ करती हैं, अंग-प्रत्यंग को श्रमकौशल से निर्मित करती और पूरा ढांचा खड़ा करके उसे अभेद्य कवच में कस देती हैं।
मां भगवती के और भी कई महान् विग्रह हैं, पर उनका अवतरण कराना अधिक कठिन रहा और भू-पुरुष के क्रम-विकास में वे उतनी स्पष्टता के साथ सामने आये भी नहीं हैं। उनमें अवश्य ही कुछ विग्रह ऐसे हैं, जो विज्ञान-सिद्धि के लिये अगत्या आवश्यक हैं — सर्वापेक्षया अधिक आवश्यक वह है जो माता के परम भागवत प्रेम से प्रवाहित होनेवाले रहस्यमय परम उल्लासमय आनंद का विग्रह है, यह वह आनंद है जो विज्ञान चैतन्य उच्चतम शिखर और जड़-प्रकृति के अधस्तम गह्वर के बीच का महदन्तर मिटाकर दोनों को मिला सकता है, अनुपम परम दिव्य जीवन की कुञ्जी इसी आनंद के पल्ले है और अब भी यही आनंद अपने गुप्त धाम से विश्व की अन्य सभी महाशक्तियों के कार्य का सहारा बना हुआ है। परंतु मानव प्रकृति बद्ध, अहंतायुक्त और तमोग्रस्त होने के कारण इन महती सत्ताओं को ग्रहण करने या उनके प्रचण्ड कर्म का आधार बनने में असमर्थ है। जब ये चार महाशक्तियां रूपांतरित मन, प्राण, शरीर में अपनी सुसंगति और मुक्त गति प्रस्थापित कर लेंगी, तभी वे अति दुर्लभ इतर शक्तियां पार्थिव गतिधारा में प्रकट हो सकती हैं और विज्ञान-कर्म संभव हो सकता है। कारण माता के सब विग्रह जब उनके अंदर एकत्र होकर प्रकट होते, उनकी भिन्न-भिन्न कर्मधाराएं एक ही सुसंगत ऐक्य में परिणत होती और ये विग्रह उनके अंदर अपने विज्ञानमय देवस्वरूपों में उठ आते हैं, तभी माता अपनी विज्ञानमयी महाशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और तभी वे अपने अकथ अलख धाम से अपनी ज्योतिर्मयी परा सत्ताओं को बरसाती हुई नीचे ले आती हैं। तभी मानव प्रकृति बदलकर सशक्तिक देवप्रकृति बन सकती है, क्योंकि विज्ञानमय सत्यस्वरूप चैतन्य और सत्यस्वरूपा शक्ति के सभी मूल तार एकत्र हो जाते हैं और जीवन की वीणा सनातन के संगीत के साथ स्वर में स्वर मिलाकर बजने के योग्य हो जाती है।
यदि तुम यह रूपांतर चाहते हो तो अपने-आपको बिना किसी दोषदृष्टि या विरोध-बाधा के, माता और उनकी महाशक्तियों के हाथों में सौंप दो और अपने अंदर उन्हें अपना काम बेरोक करने दो। तीन चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहियें — चेतना, नमनशीलता और निःशेष आत्मसमर्पण। तुम्हें अपने मन, बुद्धि और अंतरात्मा में, हृदय और प्राण में, शरीर के एक-एक रन्ध्र तक में सचेत होना होगा, माता और उनकी महाशक्तियों तथा उनके कार्यों की सुधि रखनी होगी; क्योंकि तुम्हारी अबोधता में और तुम्हारे अचेत अंगों और अवस्थाओं में भी यद्यपि वे तुम्हारे अंदर कर्म कर सकती और करती हैं, तथापि यह बात कुछ है और जब तुम उनके साथ जीता-जागता संबंध बनाये हुए रहते हो तब वह बात कुछ और। तुम्हारी सारी प्रकृति मां का स्पर्श पाने के लिये सुनम्य होनी चाहिये — अहंमन्य अज्ञ मन की तरह संशयापन्न नहीं जो बात-बात में शंका, अविश्वास और कुतर्क किया करता और अपने प्रबोध और परिवर्तन का आप ही शत्रु होता है; अपनी ही चाल से चलनेवाले प्राण की तरह हठी नहीं जो प्रत्येक भागवत प्रभाव के विरुद्ध अपनी प्रतिकूल कामना और दुर्वासना को प्रतिनियत किया करता है; मनुष्य की उस भौतिक चेतना की तरह रुकावट डालनेवाले और अक्षमता, जड़ता और तामसिकता में गड़े रहनेवाले नहीं जो आगे बढ़ने का रास्ता रोके रहती और अपनी ही क्षुद्रता और अंधता की मस्ती में आसक्त रहती हुई ऐसे प्रत्येक सत्स्पर्श के विरुद्ध चिल्ला उठती है जो निर्जीव जीवनक्रम में या उसके निष्प्राण आलस्य और घोर निद्रा में बाधक होता है। अपनी अन्तर्बहिःसत्ता निःशेष समर्पित कर देने से तुम्हारे अंग-प्रत्यंग में वह नमनशीलता आ जायेगी; और उस ज्ञान और ज्योति की ओर, उस महाशक्ति की ओर, उस सामंजस्य और सौंदर्य की ओर, उस संपूर्णता की ओर, जिनके प्रवाह ऊपर से बहे चले आते हैं, सतत उद्घाटित करते रहने से चैतन्य तुम्हारे अंदर सर्वत्र जाग उठेगा। शरीर तक जाग उठेगा और अंत को उसकी चेतना विज्ञान की परमा चिच्छक्ति के साथ एक हो जायेगी — उससे अलग कोई नीचे की चीज न रहेगी, शरीर माता की सब शक्तियों को अपने ऊपर से और नीचे से और अगल-बगल चारों ओर से अपने अंदर प्रवाहित और ओत-प्रोत परिप्लुत अनुभव करेगा और परम प्रेम और परमानन्द से पुलकित होता रहेगा।
परंतु सावधान, अपने इस क्षुद्र पार्थिव मन से माता को समझने और परखने की चेष्टा मत करो। मन का यह स्वभाव है कि यह अपने नाप और मान से, अपने संकीर्ण तर्क वितर्क और प्रमादी धारणा से अपने अथाह, दर्पभरे अज्ञान और अपने तुच्छ ज्ञान की सर्वोपरि मान्यता से समझना और परखना चाहता है उन चीजों को जो सर्वथा उसकी कक्षा से बाहर हैं। धुंधला-सा प्रकाश पानेवाली अंधता के बन्दीगृह में आबद्ध मन भागवती शक्ति के पदविक्षेपों की अबाध गति को बहुधा नहीं समझ-बूझ सकता। मन की लुढ़कती-पुढ़कती समझ माता की दृष्टि और कर्म की द्रुत गति और विविधता का अनुसरण नहीं कर सकती, उनकी गति का मान मानवी मन का पैमाना नहीं है। माता के बहुविध विभिन्न रूपों के द्रुत परिवर्तन, उनके छन्द-निर्माण और छन्द-भंग, उनकी क्षिप्रता के द्रुत वेग और उनके गतिरोध, किसी की समस्या का विचार किसी प्रकार से तो किसी दूसरे की समस्या का विचार किसी दूसरे प्रकार से — ऐसे उनके नानाविध मीमांसा-प्रकार, उनका कभी एक धागे को उठाना और फिर तुरत रख देना और दूसरे धागे को उठाना-रखना और इस तरह सब धागों को एक सूत्र में ग्रथित करना, इन सब बातों को ठीक तरह से न समझने के कारण घबराया हुआ मन नहीं देख सकता कि कैसे परमा शक्ति अज्ञान की इस गहनता को भेदकर चक्कर काटती हुई बड़ी तेजी के साथ ऊपर परमा ज्योति की ओर चली जा रही है। इसलिये यही अच्छा है कि तुम अपनी अंतरात्मा उनकी ओर खोल दो और यही यथेष्ट है कि अपनी चैत्य प्रकृति के द्वारा उन्हें अनुभव करो और चैत्य दृष्टि से उन्हें देखो, ये ही सत्य के सम्मुख होते और उसके इशारे पर चलते हैं। तब माता स्वयं ही तुम्हारे मन, हृदय, प्राण और शरीर चेतना को उनके चैत्य तत्त्वों के द्वारा प्रबुद्ध कर देंगी और अपनी रीति-नीति और प्रकृति भी दिखा देंगी।
अज्ञ मन का फिर यह आग्रह होता है कि भागवती शक्ति को सब काम, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के संबंध में जैसी हमारी थोथी मोटी समझ है, उसके अनुसार ही सदा करना चाहिये; ऐसी भूल से भी तुम बचे रहो। कारण हमारा मन व्याकुल रहता है प्रत्येक अवसर पर अद्भुत करामात, अनायास सिद्धि और चकाचौंध करनेवाला जगमग प्रकाश ही देखने के लिये; अन्यथा उसे यह विश्वास ही नहीं होता कि यहां भगवान् विराजते हैं। माता अज्ञान के साथ बरत रही हैं अज्ञान के ही क्षेत्र में, जहां वे उतर आयी हैं, सर्वथा ऊपर ही नहीं हैं। अपने ज्ञान और शक्ति को वे अंशतः छिपाये रहती और अंशतः प्रकट करती हैं, अनेक बार अपने यंत्रों और विभूतियों पर उन्हें प्रकट नहीं होने देतीं और जिज्ञासु मन, अभीप्सु अंतरात्मा, युयुत्सु प्राण तथा पाशबद्ध दुःखी पार्थिव प्रकृति के रास्ते से ही चलती हैं, जिसमें वे इन सबको रूपांतरित कर सकें। कुछ ऐसे विधान हैं जो एक परमा इच्छाशक्ति के द्वारा ही निर्दिष्ट हैं जिनका पालन करना होगा; बहुत-सी ऐसी जटिल ग्रंथियां हैं जिन्हें खोलना होगा, वे अकस्मात् काट नहीं डाली जा सकतीं। इस क्रमविकास-शील पार्थिव प्रकृति पर असुर और राक्षस अधिकार जमाये हुए हैं, उन्हीं के दीर्घकाल से अधिकृत गढ़ और प्रदेश में उन्हींकी शर्तों पर उनका सामना करके उन्हें जीतना होगा; हमारे अंदर जो मानव-भावापन्न जीव है उसे ले चलना और प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह अपनी बद्धताओं को पार करे। वह इतना दुर्बल और तमोग्रस्त है कि वह अकस्मात् किसी ऐसी स्थिति में नहीं उठाकर लाया जा सकता जो स्थिति उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत ऊर्ध्व है। भागवत चैतन्य और शक्ति मौजूद हैं और प्रति क्षण साधन-पथ में जब जो कुछ आवश्यक है उसे करते हैं, सदा-सर्वदा यथानिर्दिष्ट पदक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और अपूर्णता के बीच में भावी पूर्णता को ही साधित करते हैं। पर विज्ञानशक्ति का विज्ञानमयी प्रकृतियों के साथ साक्षात् व्यवहार तभी बन सकता है जब तुम्हारे अंदर विज्ञान अवतीर्ण हो लेगा। यदि तुम अपने मन के पीछे चलोगे तो मन माता को, उनके तुम्हारे सामने प्रकट होने पर भी नहीं पहचान सकेगा। पीछे चलो अपने अंतरात्मा के, मन के नहीं; उस अंतरात्मा के जो सत्य के अनुकूल होता है, उस मन के नहीं जो बाहरी दिखावे पर उछला करता है; भागवती शक्ति का भरोसा करो, वे ही तुम्हारे अंतःस्थ देवोचित तत्त्वों को मुक्त करेंगी और उन सबको भागवती प्रकृति की अभिव्यक्ति के रूप में ढाल देंगी।
विज्ञानमय रूपांतर भगवनिर्दिष्ट है और पार्थिव चेतना के विकासक्रम से उसका होना अनिवार्य है; कारण इसकी ऊर्ध्वमुखी गति समाप्त नहीं हुई है, मन ही इसका सर्वोच्च शिखर नहीं है। परंतु इस रूपांतर के होने, रूप ग्रहण करने और चिरस्थायी होने के लिये यह आवश्यक है कि नीचे से उसके लिये पुकार हो ऐसी उत्कण्ठा के साथ कि जब वह ज्योति अवतीर्ण हो तो उसे पहचाने, स्वीकार करे, अस्वीकार न करे; साथ ही यह आवश्यक है कि इसके लिये ऊपर से भगवान् की अनुमति हो। इस अनुमति और इस पुकार के बीच जो शक्ति मध्यस्थता का काम करती है वह भागवती माता की सत्ता और शक्ति है। केवल माता की ही शक्ति, कोई मानवी प्रयास और तपस्या नहीं, आच्छादन को छिन्न और आवरण को विदीर्ण कर पात्र को स्वरूप में गढ़ सकती हैं और इस अंधकार और असत्य और मृत्यु और क्लेश के जगत् में ला सकती हैं सत्य और प्रकाश और दिव्य जीवन और अमृतत्व का आनंद।